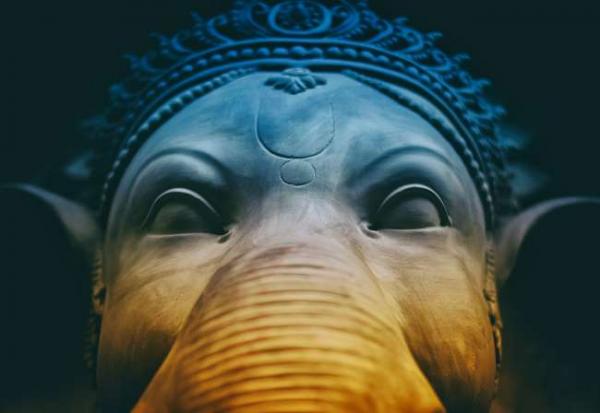वो लॉकडाउन के दो महीने

एक बंद कमरे की खिड़की से
देखता रहा सूनी सड़कें, खाली गलियाँ,
आसमान भी जैसे सहमा हुआ,
परिंदा भी कोई उड़ता न दिखता था।
एक PG का अकेला कमरा,
दूर शहर में अपने ही साथ कैद,
ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई परिचित आवाज़—
बस मोबाइल पर उभरती खबरें,
हर पल मन में घुलता एक डर।
कभी खाँसी आती, कभी ज़रा बुखार लगता,
तो दिल धड़कने लगता तेज़,
क्या ये कोविड का दस्तक है?
अगर हुआ भी तो—
कौन आएगा पास, कौन थामेगा हाथ?
दिन में सिर्फ़ दो घंटे का बाजार,
चेहरों पर मास्क, आँखों में शक,
दो गज की दूरी, आधा सामान,
टमाटर, प्याज़, आटा जैसे
छोटे-छोटे सपनों का मोल
अचानक आसमान छूने लगा था।
शामें काटने दौड़ती थीं,
रातें और लंबी हो जाती थीं—
अकेलापन बिस्तर के पास
चुपचाप आकर बैठ जाता,
कोई गाना, कोई किताब, कोई वेब-सीरीज़
उसका साया दूर नहीं कर पाती।
घर से दूर होने की टीस,
अपनों की चिंता,
खुद की असुरक्षा,
यहाँ तक कि सोशल मीडिया की
अनंत स्क्रॉलिंग भी
उस बेचैनी को मिटा नहीं पाती।
बार-बार सोचा,
क्या यही जीवन है, क्या यही सत्य है?
इतने लोग, इतनी दुनिया, फिर भी इतना अकेलापन—
क्या ये लॉकडाउन सिर्फ एक बीमारी का नहीं,
हमारे भीतर के अकेलेपन का प्रतिबिंब था?
दो महीने बीते,
खिड़की से फिर देखा—
सड़कें थोड़ी जीवंत हुईं,
कुछ आवाजें सुनाई दीं,
आसमान फिर मुस्कुराया।
पर दिल की एक कोठरी में
वो अकेलापन अब भी चुपचाप बैठा है,
एक लॉकडाउन की स्मृति बनकर,
एक अदृश्य महामारी की तरह।
रचना शेयर करिये :