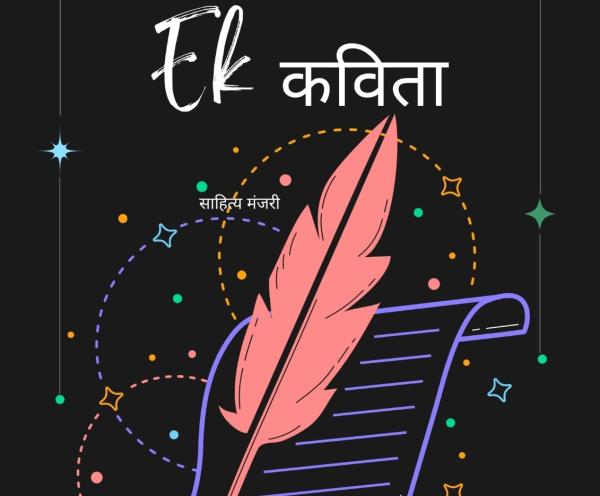ख़ाली दीवारों का शोर

(यह कविता मेरे उस मित्र की पीड़ा को स्वर देती है जिसने पाँच वर्षों में अपने पिता, माँ और पत्नी को खो दिया—अब उसका संसार केवल उसके छह साल के बेटे में सिमट गया है।)
अब ये घर नहीं, यादों का खँडहर है,
जहाँ हर दीवार से ख़ामोशी, पपड़ी बन कर झरती है।
रंगों की बात पुरानी हुई, अब तो दरारें भी थक गई हैं,
उनमें बस एक सर्द हवा, बीती हुई बातों सी सिसकती है।
एक-एक कर वो चेहरे बुझ गए,
पिता, जिनका अख़बार अब भी मेज़ पर है, बेआवाज़,
माँ, जिनके हाथ की बनी आख़िरी अचार की बरनी में,
अब तक एक उदास महक ठहरी है,
और तुम... तुम्हारी साड़ी से आती वो हल्की सी ख़ुशबू,
जो अलमारी खोलते ही, मेरे अंदर कुछ तोड़ जाती है।
अब इस सूने आँगन में,
बेटे की हँसी तीर की तरह लगती है,
उसकी हर किलकारी में, तुम्हारी हँसी की गूँज है।
और उसका वो सवाल, "पापा... मम्मी कब आएगी?"
हथौड़ा नहीं, वो एक महीन सा काँच का टुकड़ा है,
जो हर बार मेरे हलक़ में अटक जाता है।
ज़िंदगी अब कोई उजाड़ मैदान नहीं,
बल्कि एक ठहरा हुआ, गंदला पानी है,
जिसकी सतह पर मैं हर रोज़,
डूबते हुए अक्सों को देखता हूँ।
बीमारी अब जिस्म में नहीं, रूह में ज़ंग सी लगती है,
जो हौले-हौले मेरे होने को ही खा रही है।
दीवारों पर जो काई उग आई है,
वो मेरे ही आँसुओं की नमी से शायद ज़िंदा है,
हर स्मृति अब एक बर्फ़ीला ख़ंजर है,
जो मेरे आज को हर पल कुरेदता है।
बेटे की आँखों में अभी भविष्य की एक लौ टिमटिमाती है,
और मेरी आँखों के अँधेरे में,
बस अतीत की राख उड़ती है।
मैं डरता हूँ, कहीं मेरी साँसों की आँधी,
उसकी इस नन्ही सी लौ को बुझा न दे।
सुबह आती है, पर उम्मीद लेकर नहीं,
बस एक और दिन का बोझ लेकर,
एक और बार ज़िंदा रहने का अभिनय करने का आदेश लेकर।
ये घर अब घर नहीं, एक अंतहीन रात है,
जहाँ बस मैं, मेरा बेटा, और तीन ख़ामोश परछाइयाँ रहती हैं।
रचना शेयर करिये :